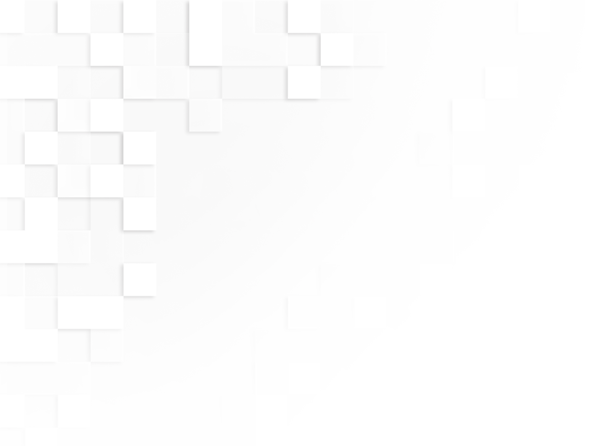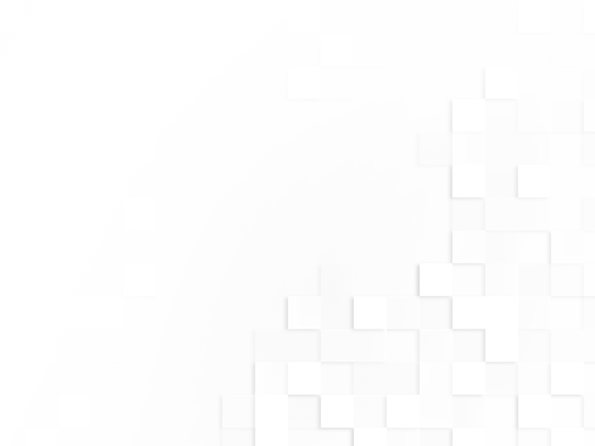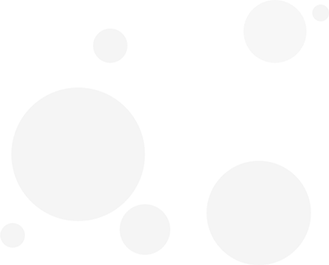प्राक्कथन
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वर्ष 1929 में स्थापना के बाद से अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रदर्शन और देश में, सभी आयामों में कृषि को मजबूत बनाने के लिए सक्षम मानव संसाधन विकसित करने हेतु कृषि अनुसंधान, उच्च शिक्षा और सीमावर्ती विस्तार पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करता आ रहा है। कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने बढ़ती खाद्य मांग के बराबर आपूर्ति को कायम रखने के लिए विभिन्न फसलों और वस्तुओं के उत्पादकता और उत्पादन में कई गुना वृद्धि करने में सहायक रहा।
कृषि उत्पादन पर्यावरण एक गतिशील सत्ता है जो लगातार विकासमान रहता है। कृषि क्षेत्र द्वारा परिवर्तन के वर्तमान चरण में सामने करने वाला कुछ नई चुनौतियां है जैसे गुणवत्ता पानी के उपलबढ़ता में कमी,मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, जलवायु परिवर्तन, खेत ऊर्जा की उपलब्धता, जैव विविधता के नुकसान,नए कीट और रोगों के उद्भव, खेतों के विखंडन, ग्रामीण-शहरी उत्प्रवासन के साथ साथ नई आईपीआर और व्यापार के नियम।
कृषि को प्रभावित करने वाले ये परिवर्तनों को हमारे शोध परियोजना में एक बदलाव की जरूरत है। हम आधुनिक विज्ञान की क्षमता, प्रौद्योगिकी पीढ़ी के क्षेत्र में नवाचारों का प्रोत्साहन तथा एक समर्थकारी नीति और निवेश समर्थनका उपयोग करना है। कुछ ऐसे महत्वपूरएन क्षेत्र है जैसे जीनोमिक्स, आणविक प्रजनन, निदान और टीकों, नैनोप्रौद्योगिकी, माध्यमिक कृषि, कृषि यंत्रीकरण, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के प्रसार को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी पीढ़ी के बढ़ती ज्ञान एवं गहन पूंजी के तथ्य को देखते हुए बहु क्षेत्रीय एवं बहु संस्थागत अनुसंधान को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के हमारे संस्थानों को प्रौद्योगिकियों और सक्षम मानव संसाधन के विकास में प्रभावी ढंग से बदलते परिदृश्य से निपटने के लिए उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होगा।
भाकृअनुप - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोची के विज़न 2050 दस्तावेज़ की तैयारी 35 वर्ष के परिदृश्य में कृषि को प्रभावित करने वाली अतीत और वर्तमान के प्रवृत्तियों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर हुआ है जो कृषि के सतत वैज्ञानिक विकास को दिखाता है।
हम उम्मीद करते है कि आनेवाले वर्षों में विज़न 2050 कृषि संसाधन एवं विकास के प्रयासों में और देश के एक अरब से अधिक की आबादी के लिए भोजन, पोषण, आजीविका तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भविष्य में कृषि प्रौद्योगिकियों उत्पन्न करने के लिए ज़िम्मेदारी उठानेवाले युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
(एस॰ अय्यप्पन)
प्रस्तावना
भाकृअनुप - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (केमाप्रौसं) से बधाई!
भाकृअनुप –केमाप्रौसं – भारत के एकमात्र प्रौद्योगिकी संस्थान है जो मात्स्यिकी के फसल से फसलोत्तर संचालन से उक्त क्षेत्र को पूरा करते है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भाकृअनुप ), नई दिल्ली के तहत वर्ष 1957 से इस देश के सेवा में लगे है। आज, तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थातपोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन और विदेशी आय में योगदान देते हुए मात्स्यिकी को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीवंत खाद्य क्षेत्र बना दिया है।
उभरते मात्स्यिकी परिदृश्य में केमाप्रौसं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक प्रमुख मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में हम देश के अर्थ व्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षा में योगदान करने के लिए मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने पर ध्यान देता है। हमें गर्व है कि संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों ने भारत के फसल एवं फसलोत्तर मात्स्यिकी क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं भारत को प्रसंस्करित मत्स्यों का प्रमुख निर्यातक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हम देश के एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के आयातित या निर्यातीत मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों रेफरल प्रयोगशाला के रूप में भी सेवारत है। समग्रत: हम मूलत: मूलभूत, सामरिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर ध्यान रखते हुए जैव विविधता के नुकसान और पर्यावरण के प्रभावों को कम करने, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके मौजूदा मत्स्य उत्पादों और प्रभावी कचरा प्रबंधन के मूल्य संवर्धन पर ज़ोर देते है जो हमारा प्रमुख योगदान है। इसके साथ का मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग में विकास, सिफारिश तथा मत्स्यन गिअर और मत्स्य उत्पादों के मानकों का लागू भी करते है।
विज़न 2050 दस्तावेज़ के रूप में संस्थान ने एक नक्शा बनाने का पूरा प्रयास किया है।इस दस्तावेज़ की तैयारी आनंददायक रहें कि संस्थान के हर व्यक्ति ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप सेइसमें योगदान दिया जिनसे आने वाले वर्षों में संस्थान और भी मजबूत होंगे। केमाप्रौसं के तकनीकी एवं सहायक कर्मचारियों की सहायता से प्रशिक्षित एवं अनुभवी वैज्ञानिक गण उपस्थित होने के कारण मात्स्यिकी के सारे चुनौतियों का सामना करने की ताकत है। केमाप्रौसं की सफलता उनके कर्मचारियों के आत्मसमर्पण से युक्त परिश्रम के साथ अब नए उत्साह और इस परंपरा को जारी रखने के लिए 2050 की ओर बढ़ने की आशा रखती है। हम शोधकर्ताओं एवं शिक्षा के साथ नेटवर्किंग में लगे रहने में विश्वास करता है क्योंकि इनसे मत्स्यन एवं मत्स्य प्रसंस्करण के ज्ञान को सशक्त करता जिनसे राष्ट्र का फायदा होगा। एक संस्थान के रूप में हमेशा से हमने कोई भी व्यक्ति / संघटन(सरकारी/ गैर सरकारी – राष्ट्रीय – अंतर्राष्ट्रीय) को स्वागत किया है जिनको भारत के मत्स्यन या मत्स्य प्रसंस्करण के विकास में योगदान या उनके बारे में शिक्षण या फिर सहयोग देने में इच्छुक है।
मानव संसाधन विकास के मोर्चे पर, संस्थान लगातार खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और मछली प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमशीलता के विकास के लिए अपने प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञता और सलाह देने के लिए जारी रहेगा। संस्थान का लक्ष्य यह है कि नियमित रूप से और मांग पर उद्यमियों, उद्योग, समान रूप से छात्रों के लाभ के लिए मत्स्यन, मत्स्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली जैसे विषयों पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर सके। संस्थान कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय और एजेंसियों और सार्वजनिक / निजी उद्योगों के साथ मत्स्य प्रसंस्करण, मत्स्य उत्पाद या मत्स्यन के साथ साथ मानव संसाधन विकास के लिए तकनीक या सुरक्षा मानकों के विकास के पहलुओं पर लगातार बातचीत करेंगे। हम केमाप्रौसं मछुआरों, मछुआरे स्त्रीयों, ग्रामीण गरीबों और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय जैसे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से हर प्रयास कर रहे है। हम 2050 बढ़ते हुए यही सामाजिक ज़िम्मेदारी हमारी प्राथमिकता होगी।
विज़न 2050 अवधि के दौरान के परिदृश्य में अनुसंधान के विस्तीर्ण क्षेत्रों में एक पुनर्गमन है । भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र को सबसे लाभदायक और स्वस्थ आजीविका विकल्प के साथ साथ राष्ट्र के पौष्टिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देना संस्थान का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
इस सुअवसर पर केमाप्रौसं टीम डॉ एस अय्यप्पन, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) और महानिदेशक को अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। डॉ बी मीनाकुमारी, महा उप निदेशक (मात्स्यिकी) भाकृअनुप को इस देस्तावेज की तैयारी के लिए दिए हुए मार्ग दर्शन के लिए आभार प्रकट करती हूं। डॉ मदन मोहन सहायक महानिदेशक, और श्री अनिल अगरवाल, प्रधान वैज्ञानिक (मात्स्यिकी) से प्राप्त योगदान आभार से स्वीकार करते है। संस्थान के जो भी सहयोगियों ने इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए अपने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और जानकारी दे दी है, उनको भी निदेशक होने के नाते मेरे व्यक्तिगत प्रशंसा एवं आभार प्रकट करता हूं। इस संकलन को तैयार करने के लिए जो प्रयास विशेषत: डॉ निकिता गोपाल, प्रधान वैज्ञानिक के साथ कुमारी पार्वती, वैज्ञानिक ने किया है उसकी भी प्रशंसा करती हूं।
अंतत: यह आशा करती हू कि यह दस्तावेज़ के माध्यम से 2050 की ओर के इस यात्रा में संस्थान को योजना एवं कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान एवं अन्य क्रिया कलापों के द्वारा संग्रहण एवं संग्रहणोत्तर प्रौद्योगिकी में टिकाऊपन लाते हुए विशेषत: मत्स्यन समुदाय एवं सामान्य मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए लाभ देने के लिए योग्य रहेगा।
कहने कि ज़रूरत नहीं है कि जलीय खाड़ी अतीत, वर्तमान और भविष्य के वैश्विक पौष्टिक सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है और मात्स्यिकी जैसे महत्व पूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते।
रविशंकर सी एन पीएचडी
निदेशक, भाकृअनुप – केमाप्रौसं
अंतर्वस्तु
संदेश
प्राक्कथन
प्रस्तावना
प्रसंग
चुनौतियां
संचालन पर्यावरण
सुनहरे अवसर
उद्देश्यों और लक्ष्यों
आगे का रास्ता
प्रसंग
भाकृअनुप-केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (केमाप्रौसं) वर्तमान में निम्नलिखित अधिदेश के भीतर कार्य करते है:
1. मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण में बुनियादी, सामरिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान का संचालन
2. जिम्मेदार मत्स्यन के लिए ईंधन कुशल मत्स्यन पोतों और मत्स्यन गिअर का डिजाइन विकसित करना
3. बायोएक्टिव यौगिकों के वाणिज्यिक अलगाव और मत्स्य एवं मत्स्य अपशिष्ट से औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों
4. मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण के लिए अभिनव औजार और मशीनरी का डिजाइन करने के लिए और विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रायोगिक संयंत्र
5. मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान करना
6. मत्स्य के संग्रहण और संग्रहणोत्तर प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण और परामर्श सेवा उपलब्ध कराना
ऐतिहासिक दृष्टि सेदेखे जाए तो खाद्य और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संघठित उच्च शक्ति समितिके सिफारिश के अनुसार भाकृअनुप-केमाप्रौसं की स्थापना हुई थी। वह कोची में में दिनांक 29 अप्रैल 1957 को कृषि मंत्रालय के अधीन में कार्यरत होने शुरू हुआ था जो बाद में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय हो गया। 1962 में संस्थान को वर्तमान नाम दिया गया था। 01 अक्तूबर 1967 से संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन लाया गया था। संस्थान के मुख्यालय कोचीन में है और वेरावल (गुजरात), विशाखापट्टनम (आंध्रा प्रदेश) और मुंबई (महाराष्ट्र) में उनका अनुसंधान केंद्र है। संस्थान के शोध कार्य सात प्रभाग के माध्यम से करवाया जाता है 1॰ मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रभाग 2 मत्स्य प्रसंस्करण प्रभाग 3 गुणवत्ता आश्वासन और प्रबंधन प्रभाग 4 जैव रसायन और पोषण प्रभाग 5 सूक्ष्म जीव विज्ञान, किण्वनऔर जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग, अभियांत्रिकी प्रभाग, एक्सटेंशन, जानकारी और आंकड़े प्रभाग।
केंद्रीय प्रौद्योगिकी मात्स्यिकी संस्थानने आवश्यकतानुसार सक्रीय तौर पर प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतरण को लगाते हुए मात्स्यिकी के उदीयमान अवस्था से संग्रहण एवं संग्रहणोत्तर क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास एवं आधुनिकीकरण लाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। मात्स्यिकी क्षेत्र में विद्यमान गतिशील परिवर्तन से संस्थान हमेशा से संवेदनशील रहे है।
2050 में नार्स और संस्थान के एकल क्रियाकालापों के परिणाम के रूप में अधिक गतिशील और कार्यक्रम, प्रबंधन और आउटपुट के मामले में वास्तविक समय प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता की मांग की जाएगी। इनका प्रमुख तत्व पारिस्थितिकी स्थिरता, न्यायसंगत उपयोग और उपयोग, लागत प्रभावशीलता और लक्षित सामाजिक लाभ होगा।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जीवन और आजीविका पर अधिक दिखाई जाएगी। वहाँ पारंपरिक संसाधनों और अपरंपरागत संसाधनों की उपलब्धता में संभावित वृद्धि की उपलब्धता में कमी होगी। यह उत्पादन और प्रसंस्करण की वर्तमान प्रणालियों में पुन: दृष्टि डालने योग्य दिया जाता। सभी स्तरों के हितधारकों की आवश्यकताओं की मांग की जाएगी। इसलिए सुझाव नवीनतम और प्रभावी होना अनिवार्य है। इसमें खाद्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसके लिए उचित सुझाव संस्थान से लिया जाएगा। वहाँ नए सीमा क्षेत्रों में अनुसंधान जिनमें विवेकपूर्ण शोषण की आवश्यकता होगी । हरित प्रौद्योगिकी पर ज़्यादा ध्यान देगा।
मात्स्यिकी क्षेत्र में संग्रहण और संग्रहणोत्तर के संदर्भ में सामना करने वाले चुनौतियों और अवसरों को व्यस्थापित ढंग से उपयोग करते हुए और भाकृअनुप के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप केमाप्रौसं के कार्यों पर एक विस्तृत दृष्टिकोण के साथ साथ मात्स्यिकी क्षेत्र की आकांक्षाओं को प्रदान करना केमाप्रौसं विज़न 2050 का लक्ष्य है।
चुनौतियां
पिछले कुछ दशकों से वाशिकी स्टार पर विद्यमान विकास ने मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। यह मुख्यत: ऐसे मन का खोज है जो विज्ञान को वाणिज्य और उद्योग में बदल दिया। इसमें मानव जीवन के गुणवत्ता और मानक में प्रगति दिखाई देने लगा जिनके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अस्थिर शोषण पारिस्थितिक असंतुलन, तेजी से जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन जैसे नकारात्मक प्रभाव भी होने लगा।
2050 तक भारत की खाद्य संबंधी मात्रा एवं गुणवत्ता की मांग बढ़ती आबादी के कारण 1.5 बिलियन के आसपास होने की संभावना है। 2050 तक उष्णकटिबंधीय में मछली उत्पादन 40% गिरावट की संभावना हैं। 2050 तक ऊष्णकटिबंधीय प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में 40% तक घटाव आने का संभावना है। भारत का मत्स्य खपत और मत्स्य उपादों का तत्कालीन राष्ट्रीय वार्षिक औसत 2.85 किलो / कापिटा है जो 2050 तक बड़ाने की संभावना है। 1.5 बिलियन आबादी के मांग की पूरती करने के लिए उत्पादन भी ओर बढ़ाना पड़ेगा।यक करने के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र को और भी अच्छे और प्रवीण उत्पादन / संग्रहण एवं संग्रहणोत्तर तरीकों को अपनाना होगा जिससे वह जलावायु परिवर्तन के उपशमन के प्रभाव के अनुरूप बना सके।
2050 तक मात्स्यिकी क्षेत्र से मांग और क्षेत्रीय चुनौतियां बढ़ने की संभावना हैं जो निम्नलिखित है –
· जलवायु परिवर्तन मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। बढ़ते तापमान समुद्र स्तर, वायु वेग एवं तरंग क्रिया, समुद्र में पारिस्थितिकी एवं जैविकी परिवर्तन के साथ साथ मत्स्य उपलब्धता कोभी प्रभावित कर सकते है। यही नहीं प्रजाति उपलब्धता में भी परिवर्तन आयेगा। जो मत्स्य खाद्य सामाग्री के तौर पर प्रयोग करता है उसके जगह अप्रयुक्त मछलियों का प्रयोग करना पड़ेगा जो एका चुनौती बननेवाले है।
· जलीय स्रोतों के प्रयोग के लिए भौगोलिक संस्थाओं के द्वारा नया मानदंड निकाला जाएगा। इसलिए राष्ट्र को आवश्यक नीति से सज्ज रहना पड़ेगा।
· क्राफ्ट एवं गिअर के निर्माण के लिए वर्तमान सामाग्री के बदले नया सामाग्री का प्रयोग किया जाएगा।
· मत्स्यन संसाधन, जैवविविधता एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न आने केलिए संरक्षण तकनीकी के विकास एवं कार्यन्वयन के लिए मांग बढ़ेगी।
· उपपकड को कम या रोकने के अलावा सुभेद्य प्रजाति का संरक्षण, संग्रहण एवं संग्रहणोत्तर संचालन में कम ऊर्जा का प्रयोग आदि गंभीर विषय होनेवाला है।
· कम प्रभाववाला और इंधन क्षमता से युक्त मत्स्यन प्रणाली का विकास अनिवार्य है।
· खुले समुद्र में प्रयुक्त मत्स्यन फ्लीटआकार में विनिमयन लाने का कोशिश प्रत्याशित है।
· आजीविका के दृष्टिकोण से देखा जाये तो जलवु परिवर्तन के कारण तटीय संरचना का विनाश निश्चित है जिससे मत्स्यन समुदायों को नए वैकल्पिक धंधों की ओर मुड़ना होगा।
· राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अंतस्थलीय मात्स्यिकी का उन्नयन हो सकता है। कुछ दशकों में नदीय मत्स्य उत्पादन को प्रभावित करने वाला कारक जैसे प्रदूषण, विनाशकारी मत्स्यन और अधिमत्स्यन बढ़ानेवाला है जिसका प्रबंधन निवारण भी आवश्यक रहेगा।
· प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मत्सयोम का संग्रहणोत्तर संचालन के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण के तकनीक का विकास अनिवार्य है जिसके लिए संरचनात्मक उन्नयन एवं पुनर्गठन भी अनिवार्य है।
· संग्रहणोत्तर संचालन एवं मूल्य वर्धित सामग्रियां अधिक मात्रा का कचड़ा को छोड़ते है जिसका प्रबंधन स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के लिए वैज्ञानिक रूप से करें। मात्स्यिकी अपशिष्ट एक गंभीर मामला के साथ साथ एक अवसर है। यानी एक ओर वह प्रदूषण का एक स्रोत है तो दूसरी ओर उच्च मूल्य वर्द्धित उत्पाद है। सही तकनीक के प्रयोग से इसका उचित प्रयोग उहच वरद्धित उत्पाद के रूप में प्रयोग कर सकते है।
· बढ़ती आबादी मत्स्य की बढ़ती मांग में परिणत होगा जिससे वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य में भी वृद्धि दिखेगा। तब इसके गुणवत्ता, सुरक्षा और अपव्यय की रोकथाम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा।
· पर्यावरणीय प्रदूषण, प्रसंस्करण में अधिक रासायनिक प्रयोग, मूल्य वर्द्धन और पारिस्थितिकी परिवर्तन के दौरान रूप लेने वाला रोगाणु आदि समुद्री खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मुद्दों के लिए नया चुनौती है।
· जल एवं ऊर्जा खपद एवं हरित गृह वातक रिहायत में पारिस्थितिकी मामलों को कम करने हेतु उत्पादों एवं प्रकीयाओं का जीवन काल मूल्यांकन अनिवार्य हो जाएगा।
· मत्स्यन, मत्स्य पूर्व – प्रसंस्करण और प्रसंस्करण क्षेत्र में सकुशल श्रमिक की गैर उपलब्धता भी अपेक्षित है।
· राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति भी यही स्थापित करते है कि जलवायु परिवर्तन, संरक्षण एवं पारिस्थितिकी का द्रुत परिवर्तन का प्रभाव मात्स्यिकी क्षेत्र पर भी दिखाई देगा।
· परंपरागत प्रणाली का तकनीकी अंतरण के कारण सार्वजनिक - निजी साझेदारी में बहुत परिवर्तन हो सकता है जिससे इसका वाणिज्यिकीकरण ज़्यादा गतिशील एवं सही मायने में दो तरह की प्रक्रिया बनेगी।
· बौद्धिक संपति की सुरक्षा के दौरान विवेकपूर्ण व्यावसायीकरण की आवश्यकता एवं सामाजिक आवश्याकताओं के प्रतिक्रिया के तौर पर नया चुनौती प्रकट होने लगेगा।
परिचालनार्थ वातावरण
भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र एक बड़ी मात्रा के परिवार को रोजगार एवं आजीविका कमाने का अवसर प्रदान करता है। मत्स्य गुणवत्ता प्रोटीन के स्रोत होने के साथ वसा एवं विटामिन एवं मिनरल का भी स्रोत है जिसके कारण मानव पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। भारत प्राकृतिक जल संपदाओं से सम्पन्न है जिसके कारण यह क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गए।
राष्ट्रीय स्तर पर मात्स्यिकी नीतियां बड़े पैमाने पर विकसित एवं कार्यान्वयन में ला रहे है जिसकी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। वर्ष 2050 तक ये नीतियां जो राज्य स्तर सीमित है बेहतर मात्स्यिकी प्रबंधन के लिए वह एकीकृत किया जाएगा। यह सब जलवायु परिवर्तन, संपदा संरक्षण की आवश्यकता, बढ़ती मत्स्य खपत के इस युग में स्वास्थ्य सुरक्षा के कारण प्रति व्यक्ति खपत बढ्ने वाले है। बदलते जीवन शैली और शहरीकरण के परिणाम स्वरूप मत्स्य उत्पाद के लिए मांग बढ़नेवाले है। बढ़ती आबादी पारिस्थितिकी प्रदूषण एवं नए उपादों का परिचय कड़ी से कड़ी गुणवत्ता आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों की मांग को पैदा करती है।
नवीकृत संचालन पर्यावरण में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय भागीदरों जैसे मात्स्यिकी विभाग, मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्य उपभोक्ता, अन्य विज्ञान एवम प्रौद्योगिकी सम्स्थान और निजी क्षेत्र के अलावा हितधारक राष्ट्र के मछुआरे ही होगे.
मत्स्यन गिअर और अभ्यास के ऐतिहासिक उत्क्राम्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विकास 1. क्राफ्ट प्रौद्योगिकी में संचालक शक्ति, गिअर एवम पकड तरीकों में विकास 2. कृत्रिम गिअर सामग्री का विकास 3 मत्स्य खोज में विकास 4.इलेक्ट्रोनिक नौचालन के क्षेत्र में प्रगति 5. जिम्मेदार मत्स्यन की आवश्यकता को अवगत कराना और जैवविविधता के परिरक्षण के साथ साथ पर्यावरणीय सुरक्षा. तटीय क्षेत्र के बीच के अत:क्षेत्रीय भेदभाव के परिणाम स्वरूप, जिम्मेदारी मत्स्यन अभ्यास और पकड मात्स्यिकी विकास में सावधान की ज़रूरी अनिवार्य है. भारत में अधिमत्स्यन और अध: मत्स्यन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. अधिमत्स्यन को निकालने से और जिम्मेदार मत्स्यन गिअर को अपनाने से नकारात्म्क पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, जैव विविधता की रक्षा करना और संसाधनोम की टिकाऊपन में सहाय रहेगा.
अन्य बहुत सारे पकड प्रणालियाँ होते हुए भी हाल में उसकी गति में फीका पड गया. पानी अमूर्त पर्यावरण क्षरण, नदी के किनारों की वृद्धि की अवसादन नदीय संसाधनों के लिए हानिकारक है. भारत के नदीय संसाधन अति क्षमता से युक्त है जिसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार मत्स्यन, कण आकार को नियमित रूप से बनाना इष्टतम मत्स्यन प्रयास जैसे उचित प्रबम्धन उपाय से की जा सकती है. इतना प्रौद्योगिकीकरण के बावजूद आज भी भारतीय मात्स्यिकी में वैज्ञानिकी तौर का हस्तक्षेप बहुत कम है. अत:स्थलीय जलाशयों में अभी भी परम्परागत मत्स्यन उपकरणोँ का प्रयोग होता है. विष एवम विस्फोटकोम से प्रयुक्त मत्स्यन आज भी विद्यमान है. वैश्विक रूप से एवम भारत में जलीय कृषि सबसे गतिमान खाद्य उत्पादन क्षेत्र है. जलीयकृषि उत्पादो का प्रमाणीकरण एवम इकोलेबलिम्ग सही तौर पर किया जाये तो इसके विकास के लिए लाभदायक होगा.
आबादी के महत्वपूर्ण विभाग के अतिजीवनएवम स्वास्थ्य में मत्स्य महत्वपूर्ण योगदान है. वर्ष 2050 होते होते बढती आबादी के साथ मत्स्य खाद्य सुरक्षा की माम्ग बढ्ती जाएगी. प्रोटीन की माम्ग की आपूर्ति के लिए मत्स्य का खपत होने लगेगा. भारतीय आबादी को इसके बारे में अवगत करना अनिवार्य होगा. खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवम आर्थिक मामला है. मुफ्त वाणिज्य की दृष्टिकोण से देखा जाये तो मत्स्य एवम उसकी सुरक्षा चिंता का विषय है. खाद्य संबंधी रोग एवम आपूर्ति श्रृंगला के विविध रोगाणु के उत्भव भी चिंता का विषय है.
प्रौद्योगिकी विकास एक सरल प्रक्रिया नहां है. उसमें बहुत सारे कदम शामिल है जैसे पूर्व मूल्यांकन, योजना, कार्यांवयन, मूल्याम्कनोत्तर . क्षेत्रानुसार इसका समय बदलता रहता है. प्राय: प्रौद्योगिकी में निरंतर निगरानी और हितधारकों से निरंतर अंत:क्रिया होना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र भी मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी में शामिल है जिससे क्षेत्र को भी लाभदायक हो रहा है।
ज्ञात स्वास्थ्य कारणों के लिए मछली की खपत में वृद्धि के समय में, मछली की प्रति व्यक्ति खपत आगे बढ़ाने की संभावना है। बदलती जीवन शैली और अत्यधिक शहरीकरण और मानव मुद्रा और बढ़ाया व्यापार को आगे बढ़ने के संदर्भ में नवीकृत उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से मत्स्य आधारित उत्पादों के लिए मांग की वृद्धि होने की संभावना है। बढ़ते प्रदूषण के परिणाम स्वरूप होने वाले संदूषण और नए उत्पादों उच्च गुणवत्ता आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों की मांग करती है।
अवसर
विज़न
संग्रहण एवं संग्रहणोत्तर प्रौद्योगिकियों में नवाचारों के माध्यम से टिकाऊ संग्रहण और मात्स्यिकी संसाधन का कुल उपयोग को सुविधाजनक बनाना।
मिशन
पर्यावरणनुकूल, ऊर्जा से भरपूर, आर्थिक साधन के माध्यम से मात्स्यिकी संसाधन के जिम्मेदार संग्रहण का सुनिश्चयन करना; उचित प्रसंस्करण, मूल्य वर्द्धन, पैकेजिंग, और अपशिष्ट उपयोगीकरण का सुनिश्चयन; उपभोक्ता को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा का सुनिश्चयन करना इनका मिशन है।
फोकस
उपर्युक्त विज़न एवं मिशन को उत्तीर्ण करने के लिए केमाप्रौसं निम्न प्रकार कार्य करेंगे:
· पकड़ एवं मात्स्यिकी पालन के लिए जलवायु परिवर्तन अनुक्रियाशील और प्रतिस्थिति मत्स्यन प्रणाली का विकास
· संग्रहीत मात्स्यिकी संसाधन के उपयोगीकरण केलिए प्रौद्योगिकी उपाय का विकास
· मत्स्यन में हरित, अक्षय पुनरावृत्तीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का परिचय
· जैव पूर्वेक्षण और जलीय के जीनोमिक्स के अवसरों को प्रयुक्त करना
· सुरक्षित मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और खपत के सुनिश्चयन के लिए पारंपरिक और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का विकास
· पशु स्वास्थ्य संबंधित मामलों के सुझाव के लिए उचित जैव-सुरक्षा उपायों का विकास
· नवीकृत प्रौद्योगिकी अंतरण और व्यावसायीकरण मॉडल की विकास के लिए नया प्रौद्योगिकी
· उचित क्षमता निर्माण के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना।
जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव
जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप भविष्य में प्रजातियों के प्रादेशिक उपलब्धी पर अच्छा या बुरा प्रभाव देख सकता है। जलवायु परिवर्तन एक मूर्त घटना एवं पर्यावरण को प्रभावित करने का साधन होने के कारण हरित प्रौद्योगिकी के ऊपर इसका दबाव बढ़ रहा है। क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में यह सहायक रहेगा,। जलवायु परिवर्तन के परिणामों को लंबे समय तक सामना करने की क्षमता से युक्त प्रौद्योगिकी को विकास करना चाहिए।
संग्रहण एवं संग्रहणोत्तर मात्स्यिकी के लिए हरित ईंधन
पकड़ मात्स्यिकी, जलीय कृषि और संग्रहणोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में होती है। नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर, पवन, विद्युत, ज्वार आश्रित करने वाले हरित प्रौद्योगिकी ऊर्जा का उपयोग कम करने के साथ क्षेत्र के क्षमता को कम करते है। जलीय जीवों आधारित जैव ईंधन घटती जीवाश्म ईंधन संसाधनों के लिए एक आकर्षक विकल्प हैं और स्थिरता में सुधार और जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास हरी ईंधन के उत्पादन के लिए एक आर्थिक और पारिस्थितिकी टिकाऊ पैमाने स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। ऊर्जा बजट मत्स्य पालन गतिविधियों में एकीकृत किया जाना आवश्यक है।
पकड मात्स्यिकी: मत्स्यन प्रणाली, सामग्री और पालन
पकड़ मात्स्यिकी क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसाधन, जाइवावीधता और पर्यावरण पर मात्स्यिकी का नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु पालन प्रौद्योगिकी का विकास एवं कार्यान्वयन की मांग बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को शमन करना भी अनिवार्य होगा जिसके कारण से प्रजाति के उपलब्ध्ता पर असर होगा। स्वयं पर्याप्त ऊर्जा पोत की संकल्पना वास्तविक में होगा और ऐसे प्रणाली का रचना और विकास भी आवश्यक है। राष्ट्रीय तौर पर हर मत्स्यन प्रणाली को विकास करने का मानक का परिचय भी किया जाएगा।
उपपकड़ के लिए भी प्रौद्योगिकी का विकास भी अनिवार्य है। जलीय संसाधन के प्रयोग के लिए उपयुक्त उपकरण एवं फ्रेमवर्क के वैश्विक तौर पर स्वैच्छिक और अनिवार्य दिशा निदेशों की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में जलाशय मात्स्यिकी के उच्च क्षमता के कारण उसको और बढ़ावा मिलेगा। असल में जलाशय मात्स्यिकी को बेहतर पालन और प्रबंधन उपाय की ज़रूरत है। प्रदूषण, हानिकारक मत्स्यन और अधिमत्स्यन जैसे कारक जो जलाशय मात्स्यिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उससे बचने के लिए प्रबंधन निवारण की आवश्यकता भी उत्पन्न होगा।
जलाशय प्रणालियों का प्रदूषण
क्राफ्ट और गिअर के नव सामाग्री के परिचय से परिणत नानो एवं सब-नानो सामग्रियों से रूपायित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए न्या प्रबंधन, शमन एवं उपचार रणनीति उपयुक्त होगा। नए सामाग्री से उत्पन्न जैव अवरोध एवं गिरावट को रोकने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और तकनीक भी आवश्यक होगा जिसमें जैव प्रौद्योगिकी उपकरण के जैव उपायकरण कर सकते है।
मत्स्यन प्रणालियों से उत्पन्न प्रदूषण भी चिंता का विषय है जैसे उप पकड़ का अपशिष्ट, ऑन बोर्ड प्रसंस्करण, अनुपयोगी मत्स्यन गिअर, ईंधन अपशिष्ट और पोत संचालन से उत्पन्न उत्सर्जन आदि। प्रभावी नीति निर्माण के द्वारा निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण को भी बेहतरीन बनाना होगा।
मात्स्यिकी में उच्च क्षमता एवं वांछनीय विशेषता होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग और भी जारी रहेगा। फिर भी ये सबसे गैर जैवनिम्नीकृत सिथेटिक सामाग्री है जो मात्स्यिकी के लिए ही नहीं पूरे पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक खतरा है। भविष्य में इसको शमन करने वाले उपाय लेना भी अत्यधिक आवश्यक बनेगा।
जलीय खाद्य उत्पादन प्रणालियों में जोखिम का मूल्यांकन
खुले समुद्र मत्स्यन और जलीय कृषि में अधिक नियंत्रण युक्त मत्स्य उत्पादन आवश्यक होगा। विदेशी प्रजातियों का परिचय द्वारा नया रोग आदि आने की संभावना भी दिखाई देता है। ऐसे परिस्थिति से बचाने के लिए जलीय कृषि और समुद्री कृषि का निरंतर निगरानी की आवश्यकता है । उभरते रोगजनकों के बारे में विस्तृत ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
मानवीय संसाधन
जवायु परिवर्तन, व्यवसाय, जैव विविधता, पर्यावरण, से संबंधित निर्णय लेने और अनुसंधान में नए मॉडल और तकनीक को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए वैज्ञानिको को प्रशिक्षण देना होगा। इसके साथ हितधारकों को भी को भी ऐसे चुनौतियों के सामना करने के लिए तैयार रहना होगा जो पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकीय बदलाव से उभर आते है।
उद्देश्यों और लक्ष्यों
नार्स के अविभाज्य अंक होने के नाते संस्थान का मुख्य कार्य मात्स्यिकी के संग्रहण और संग्रहणोत्तर क्षेत्र के प्रौद्योगिकी विकास का अनुसंधान है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान केन्द्रित क्षत्र निम्नलिखित होगी।
· मात्स्यिकी संसाधन के उपयोग के लिए मानकीकृत हरित मत्स्यन प्रणाली
· संग्रहीत संसाधनों के सम्पूर्ण उपयोग के लिए संग्रहणोत्तर प्रौद्योगिकी और उपाय
· जलीय रोग प्रबंधन, जैव उपायीकरण जैसे अनुप्रयोगों पर आधारभूत अनुसंधान
· सुरक्षित मत्स्य उत्पादन के लिए गुणवत्ता प्रणाली
· हितधारकों के बीच में प्रभावी एवं सक्षम प्रौद्योगिकी अंतरण
अगले चार दशकों तक संस्थान ने निम्नलिखित लक्ष्यों को उत्तीर्ण करने का प्रयास करने वाले है :
· पारिस्थितिकी अनुकूल मत्स्यन प्रणाली के साथ उभरते प्रजातियों के लिए मानकीकृत क्राफ्ट गिअर का सम्मिलन
· क्राफ्ट एवं गिअर एवं पकड़ के निगरानी के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी, सेंसर, कैमरा और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का एकीकरण
· पकड़ मात्स्यिकी द्वारा लक्षित प्रजाति उत्पादन के लिए पूर्व-सूचना मॉडल का विकास
· संसाधन पालन के लिए पकड़ सहायक प्रौद्योगिकी का विकास
· पर्यावरण प्रमाणित स्थिति को प्राप्त करने पर छोटे पैमाने पर कार्यरत गैर मोटोरीकृत परंपरागत नायिका समुदाय पर रोकथाम
· उभरते मात्स्यिकी संबंधित मानकों के लिए नीति परामर्श
संग्रहीत मात्स्यिकी संसाधन के सम्पूर्ण उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी उपाय को उपलब्ध करवाना
· अपरम्परागत मत्स्य प्रजाति के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
· मूल्य वर्द्धित, सुविधाजनक उत्पादों के लिए उपभोक्ता चालित प्रक्रिया मोडलिंग का विकास
· द्वाओम, योजक, वैकल्पिक पोषण, अर्क, पिगमेंट, फीड के उच्च मूल्य उत्पादों के उत्पादन के लिए अपशिष्ट के प्रयोग के द्वारा ज़ीरो – लॉस प्रसंस्करण
विविध प्रयोग के लिए जैव पूर्वेक्षण और जाईय और अन्य संसाधनों के जीनोमिक्स के अवसरों का प्रयोग
· निम्नलिखित क्षेत्रों में जीनों का पहचान और निदान एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का खोज
· जलीय रोग प्रबंधन
· विशिष्ट पोषक तत्वों को शामिल कराते हुए मत्स्य पोषण की गुणवत्ता में सुधार
· पोषक तत्व उत्पादन जीन का परिचय
· पोषक तत्व को अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए बायोरीफाइनरी
· जैव उपायीकरण
सुरक्षित मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और पालन के सुनिश्चयन के लिए परंपरागत और सीमांत प्रौद्योगिकी के द्वारा गुणवत्ता
· उत्पादन से खपत तक सुरक्षित मत्स्य के लिए गुणवत्ता प्रणालियों का विकास
· बेहतरीन खाद्य सुरक्षा हेतु रासायनिक सूक्ष्मजीवविज्ञानी खतरों के लिए तीव्र खोज तरीकों
· उभरते रासायनिक और रोगाणु का जोखिम मूल्यांकन
· खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएम मत्स्य के मानकों का विकास
पशु स्वास्थ्य के मुद्दों का हल निकालने के लिए उचित जैव सुरक्षा का विकास
· उभरते खतरों के खोज के लिए जैव-प्रौद्योगिकीय, आणविक और नानों-प्रौद्योगिकीय उपकरण जैसे सीमांत प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।
· जोखिम मूल्यांकन और जलकृषि प्रणालियों के निरंतर निगरानी के द्वारा बेहतरीन जैव सुरक्षा का विकास
नवीकृत प्रौद्योगिकी अंतरण और वाणिज्यीकरण मॉडल के विकास हेतु नई प्रौद्योगिकी का दोहन
· प्रौद्योगिकी अंतरण मॉडल के विकास के लिए उभरते वेब और अन्य संचार आधारित प्रौद्योगिकियों का एकीकरण
· प्रौद्योगिकी सलाह और सामयिक डाटा प्रबंधन के माध्यम से मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण के लिए नए व्यवसाय मॉडल।
प्रणालियों के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना
· जलवायु परिवर्तन, व्यवसाय, जैवविविधता और पर्यावरण से संबंधित सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और निर्णयकर्ताओं को सशक्त करना।
· ऊष्मायन कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता विकास
· सुभेद्यता और अन्य झटकों के खिलाफ मत्स्यन समुदाय को सक्षम बनाना
आगे का रास्ता
भारतीय मात्स्यिकी के आधुनिकीकरण और मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण के विकास में केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है।
जब मात्स्यिकी क्षेत्र तत्कालीन समय में अधिक संसाधन का क्षरण और तटीय जलों में मात्स्यिकी पर्यावरण में बदलाव हो रहा है तब निचले समुद्र में अप्रयुक्त संसाधन भी उपलब्ध है जिसका विनियोग उचित प्रबंधन योजना से संभव है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव निश्चय ही मात्स्यिकी क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालने वाला है और इसका असर मछुआरों और उनके आजीविका पर भी पड़नेवाले है। इसके प्रभाव को शमन करने हेतु उचित नीति और प्रबंधन उपाय अनिवार्य है। संग्रहणोत्तर प्रौद्योगिकी के विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना अनिवार्य है ताकि जलीयकृषि और पकड़ मात्स्यिकी से आधारित अप्रयुक्त संसाधन को भी संभाल सके। समुद्री खाद्य सुरक्षा प्रणाली और घरेलू बाज़ार की ओर भी ज़्यादा ध्यान देना अनिवार्य है जिससे उभरते चुनौतियों का सामना करने में सहायक रहेगा। भविष्य के लिए संसाधन घटाव को कम करना एवं ऊर्जा पालन सबसे महत्वपूर्ण नीति उद्देश्य और प्रौद्योगिकी चुनौती होगा।
नार्स के अंक होने के नाते संस्थान ने अपना परिदृश्य वहां प्रस्तुत किया है। केमाप्रौसं उनके अद्वितीय विशेषण के कारण एक ऐसे केंद्रीय पद को अलंकृत किया है जो आगे चलकर 2050 में भारतीय मात्स्यिकी में अनेक प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के नेता बनने के सफर में है जिसके द्वारा भारत में अनेक आर्थिक विकास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों को आजीविका बना के देगा।
इस विज़न को उत्तीर्ण करने हेतु संस्थान ने जो का नीति निर्माण किया है जो निम्न प्रकार है :
अनुलग्नक I रणनीतिक फ्रेमवर्क
|
उद्देश्य
|
पहूंच
|
प्रदर्शन के उपाय
|
|
जलवायु परिवर्तन से प्रतिक्रियाशील और प्रतिस्थितित्व मत्स्यन प्रणाली में प्रगति
|
·मानकीकृत क्राफट और गिअर मिश्रण का विकास
·क्राफ्ट और गिअर एवं निचले जल पकड़ की निगरानी करने के लिए कृत्रिम उपकरण का विकास
·लक्षित प्रजाति के लिए पूरवा सूचना मॉडल का विकास
·उभरते मात्स्यिकी से संबंधित मानकों और पारिस्थितिकी प्रमाणन के लिए नीति सलाहकार
|
· अनुकूलित, संसाधन विशिष्ट पालन उन्मुख मत्स्यन प्रणाली
· वैज्ञानिक नीति आदान
|
|
उचित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संग्रहीत मात्स्यिकी संसाधन का सम्पूर्ण उपयोग
|
·मूल्य वरद्धित उत्पादों के लिए उपभोक्ता उन्मुख प्रसंस्करण मॉडल और प्रौद्योगिकी
·उच्च मूल्य उत्पादों के विकास के लिए अपशिष्ट का सम्पूर्ण उपयोग
|
· मूल्य वर्द्धित उत्पाद
· मत्स्य अपशिष्ट से उच्च मूल्य उत्पाद
· नए उत्पादों के लिए नवीकृत प्रसंस्करण
|
|
मत्स्य संग्रहण और संग्रहणोत्तर क्षेत्र में हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का प्रयोग
|
·संग्रहण और संग्रहणोत्तर क्षेत्र में उतपदाओं और प्रसंस्करण का जीवन चक्र मूल्यांकन के द्वारा कार्बन का न्यूनीकरण
·मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण के क्रियाओं को नियंत्रण करने केलिए सौरव, हवा, विद्युत और ज्वार ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा का प्रयोग
·मात्स्यिकी क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन का वैकल्पिक साधन के रूप में आलगे आधारित जैव ईंधन का प्रयोग
·प्रदूषकों को नियंत्रण करने के लिए प्रोटोकोल्स का विकास
|
· हरित मत्स्यन पोत की रचना
· मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण में ईंधन कुशल अभ्यास का इस्तमाल
· पुनरुपयोगी और पुनरावृत्रित ईंधन का प्रयोग
· मत्स्य उत्पादन और मत्स्या प्रसंस्करण में कार्बन का न्यूनीकरण
|
|
खाद्य जनित और सुसंस्कृत प्रजातियों रोगजनकों के लिए आण्विक निदान
|
·बैक्टीरियल और वायरल रोगजनकों के लिए समुद्री खाने की निगरानी
·बैक्टीरियल और वायरल रोगजनकों का पता लगाने के लिए तेजी से तरीकों।
·सुसंस्कृत प्रजातियों की बाउन्ड्री रोगों के नियंत्रण के लिए रणनीतियाँ।
·रोगजनकों / विदेशी रोगजनकों के लिए जलीय कृषि प्रणालियों की निगरानी
|
· समुद्री भोजन जनित और सुसंस्कृत प्रजातियों रोगाणुओं की व्यापकता पर डेटाबेस।
· समुद्री भोजन से जनित रोगज़नक़ों और झींगा वायरस के लिए बेहतर तरीकों का खोज
· विदेशी रोगों से स्वदेशी मछली प्रजातियों का संरक्षण।
· जल कृषि फार्मों में सुधार जैवसुरक्षा उपायों का विकास।
|
|
जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स और समुद्री बैक्टीरिया की आणविक विविधतापर अध्ययन ।
|
· पूरे जीनोम अनुक्रमण और रोगजनक जीवों की एनोटेशन।
· पाटोजेनिसिटी के लिए जिम्मेदार जीन की पहचान उपन्यास
· जैवाणुओं के लिए जैवकृत्रिम जीन समूहों की पहचान करना।
|
· रोगजनन, दवा प्रतिरोध और मेजबान परजीवी रिश्ते और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के तंत्र को समझना।
· औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ समुद्री बैक्टीरिया पर डेटाबेस।
· भोजन और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बायोएक्टिव अणुओं।
|
|
पारंपरिक और सीमांत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर गुणवत्ता प्रणाली के विकास के लिए सुरक्षित मछली उत्पादन, प्रसंस्करण और खपत का सुनिश्चयन करना
|
·मानकों, प्रक्रियाओं और यह सुनिश्चित करना है और उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल सहित खपत के लिए उत्पादन से सुरक्षित मछली के लिए गुणवत्ता प्रणाली का विकास।
·खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी खतरों के लिए द्रुत खोज लगाने के तरीकों
·उभरते रसायनों के जोखिम आकलन और उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए रोगजनकों
·खाद्य सुरक्षा के मुद्दों और जीएम मछली के लिए मानकों के विकास
|
· मछली / झींगा रोगज़नक़ के लिए कम लागत स्वदेशी निदान किट
· फार्म के लिए कांटा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) अनुकूलित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के लिए विशेष डिजाइन।
· घरेलू स्तर पर खाद्य कानून के अधिकारियों द्वारा गोद लेने के लिए मछली के लिए मानक।
· जैविक खतरों के रुझान, मत्स्य वातावरण में खतरों के स्थानिक और लौकिक भिन्नता।
· जोखिम मूल्यांकन और जीएम मछली के लिए मानकों
· पता लगाने की क्षमता के लिए जैविक (डीएनए) टैग के विकास / मछली / मछली उत्पादों के प्रमाणीकरण
|
|
पशुओं के स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए उचित जैवसुरक्षा का विकास
|
·अग्रणी प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकी आणविक और नैनो-तकनीकी उपकरणों, उभरते खतरों के तेजी से पता लगाने के लिए की तरह के अनुप्रयोग।
· जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से सुधार जैव-सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल के विकास और जलीय कृषि प्रणालियों के निरंतर निगरानी।
|
· जलीय प्रणालियों की निगरानी के लिए खतरों की पहचान के लिए रैपिड तकनीक
· रोगजनकों / विदेशी रोगजनकों के लिए जलीय कृषि प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से जैव सुरक्षा
|
|
प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के विकास
|
·प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मॉडल के विकास के लिए प्रभावी वेब आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
· परंपरागत लोगों के साथ अभिनव प्रौद्योगिकी के एकीकरण।
|
· वास्तविक समय उत्तरदायी टीओटी मॉडल
|
|
सभी सिस्टम के स्तर पर मानव संसाधन विकास
|
·ऊष्मायन कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, व्यापार, जैव विविधता और पर्यावरण और उद्यमियों से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में शोधकर्ताओं को सशक्त बनाना।
·विकासशील मॉडल और नई तकनीकों और क्षेत्र के उभरते हुए मांग के अनुसार अनुसंधान के तरीके।
|
· मात्स्यिकी क्षेत्र के चुनौतियों के सामना करने के लिए क्षमता बढ़ाना।
|